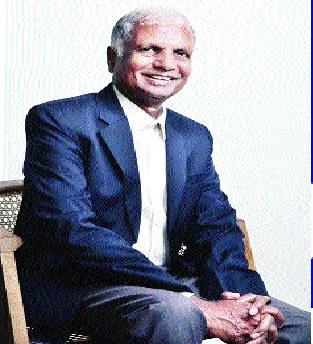
हम जीवन में जो कुछ करते हैं, उसके पीछे एक चाहत होती है। चाहत के पीछे प्रयास होते हैं और उन प्रयासों से कामयाबी या विफलता दोनों जुड़ी होती है। जो चाहत थी, वह मिल गया तो हम कामयाब हो गये और न मिला तो विफल। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि हम विफलता हासिल होने पर न तो दुखी हों और न क्रोधित। हमने अपनी चाहत को प्राप्त करने में पूरी उर्जा लगाई, नई पा सके, कोई बात नहीं, पर इस स्थिति में कुंठित होना आवश्यक नहीं है। पर मानव स्वभाव है कि क्रोध या कुंठा को रोक नहीं पाते। वस्तुत: क्रोध एक बाई-प्रोडक्ट है, जो विफलता या कुंठा से सृजित होता है। क्रोध न आये, इसके लिए जरूरी है कि हम में किसी वस्तु की चाहत इतनी तीव्र नहीं होनी चाहिये कि वह जीवन-मरण का प्रश्न बन जाये। प्रयास किया था, नतीजा हमारे पक्ष में आ गया तो अच्छा है और नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आगे आ जायेगा। यहां उक्त बातें कहने-लिखने का अर्थ यह नहीं कि हम इच्छा न करें। इच्छा नहीं करेंगे यह संभव नहीं, इच्छा जागृत होती है यह स्वाभाविक है, इच्छा प्राप्ति की दिशा में प्रयास न करें तो समानांतर एक दमन बनेगा जो इच्छा को मारने के लिए इंगित किया जाता है। सच यह है कि हम जो आकांक्षा पाल लेते हैं, तो उसके प्रति एकाकार हो जाते हैं और जब वह पूरी नहीं होती तो हमारी अपनी उर्जा ही आग सी बन जाती है और हमें जलाने लगती है। ऐसे में हम कदाचित पश्चाताप कर रहे होते हैं। विफलताएं यदि बढ़ती हैं, तो उनकी एक श्रंखला बन जाती है और हमारा पूरा जीवन उसमें संलग्न हो जाता है। यूं हजारों वर्षों से यह कहा जाता रहा है कि आकांक्षा रहित जीओ, पर क्या ऐसा संभव है। बल्कि यह तो अमानवीय स्थिति है, मनुष्य है तो आकांक्षा रहेगी, कुछ पाने की इच्छा भी। आकांक्षाओं के अपने आकार-प्रकार होते हैं, कुछ बड़ी होती हैं और कुछ छोटी भी। बड़ी आकांक्षा की प्राप्ति के लिए हम छोटी को दबा लेते हैं, बहुत बार लक्ष्य भी बदल लेते हैं, ऐसा होना स्वाभाविक है और यह मानवीय प्रवृत्ति है। यहां एक किस्सा याद आता है, एक बार तीन साधु कहीं मिले, अलग-अलग पंथ के थे। पहले ने अपने पंथ के बारे में बताया कि उनके यहां विद्वता का बहुत महत्व है और शिक्षा के लिहाज से हमारा पंथ सबसे बेहतर है। दूसरे साधु ने कहा कि आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन जहां तक तपस्या का संबंध है हमारा पंथ सबसे बेहतर है। शिक्षा केवल ज्ञान तक सीमित है और आध्यात्मिक अनुशासन तो तपस्या से ही आता है। अब तीसरे साधु की बारी थी, उसने कहा कि आप दोनों ठीक कह रहे हैं, पहला पंथ शिक्षा में अच्छा है और दूसरा आध्यात्मिक अनुशासन और तपस्या में बेहतर है, लेकिन जहां तक निरहंकारिता का सवाल है हमारा पंथ सबसे आगे है। जब बात निरहंकारिता की हो रही है, उसमें अपने आप को सबसे बेहतर बताना कितना दिलचस्प है।
इसलिए कि निरहंकारिता की बात कहना अपने आप में अहंकार का प्रकटीकरण है। पर यहां विशेष बात यह है कि इस निरहंकारिता को रोकना कभी नहीं चाहिये, क्योंकि यह एक स्वाभाविक प्रकृति या प्रवृत्ति है। क्योंकि इसे रोकेंगे तो यह मन को कचोटेगी, अत: इसे बने रहने देना चाहिये। संतों के बीच जब इस तरह का विचार-मंथन होता है, तो जाहिर होता है कि उनके भीतर विनोद भाव तो कहीं है ही नहीं, जो है वह ज्ञान, तपस्या और निरहंकारिता। किसी भी धर्म या पंथ ने क्या विनोद भाव को एक बुनियादी गुण के तौर पर स्वीकार किया है। मेरा यह मानना है कि ‘प्लेफुलनैस’ अर्थात विनोद भाव तो मानव में मूलभूत गुण होना चाहिये। हम हर बात को गंभीरता से ले जाते हैं। कभी विनोद भाव या हंसी का उपयोग भी करें। यह दुनिया बहुत बड़ी है, अरबों लोग रहते हैं, हर व्यक्ति कुछ न कुछ पाने का प्रयत्न कर रहा है, यह स्वाभाविक है। आवश्यकता इस बात की है कि हम सहजता से अपने बारे में सोचना शुरू करें, कुछ विषेष नहीं कि हम जीतने के लिए बने हैं या इच्छित वस्तु पाने के लिए बने हैं। दुनिया चूंकि बहुत बड़ी है, सभी की शत-प्रतिशत इच्छाएं पूरी हो यह जरूरी नहीं। इस सच को स्वीकार करना सबसे बड़ी स्वीकारोक्ति है। दूसरी बात यह है कि हम किसी भी चीज को बहुत गंभीरता से न लें, स्वयं को भी नहीं। जब हमारा सोच इस तरह का हो जायेगा, तो क्रोध नहीं आयेगा और कोई काम न होने पर खिन्नता नहीं होगी बल्कि मन यह कहेगा चलो कोई बात नहीं आगे हो जायेगा। जब हमारे दिल में क्रोध आता है या खिन्नता आती है, तो उससे हमारी आध्यात्मिक उर्जा का रिसाव होने लगता है, इसलिए अपनी आकांक्षाओं के प्रति प्लेफुल होना सीख लें वह महत्वपूर्ण है। बिजनस के नजरिये से इस बात का सार यह है कि कंपनियां अपने लक्ष्य निर्धारित करती हैं, हासिल हो जाये वहां तक तो ठीक है, हासिल नहीं होता तो कंपनी मालिक और प्रबंधक बहुंत चिंतित होते हैं, तनाव-ग्रस्त होते हैं और उससे जनित गुस्सा सेल्स टीम, मार्केटिंग हैड आदि पर निकलता है। उन बेचारों का क्या कसूर। उन्होंने तो अपने पूरे प्रयास किये हैं, अब कामयाबी नहीं मिली या लक्ष्य पूरे नहीं हो पाये तो इसके लिए दोषारोपण भी किसी को नहीं किया जाना चाहिये बल्कि नई तैयारी के साथ पहल की जानी चाहिये। बिजनस को लक्ष्यों को खेल की तरह लिया जाना चाहिये, जीत गये तो जिंदाबाद और हार गये तो फिर से कोशिश। फिर से कोशिश का मन रहेगा, तो नई उर्जा मिलेगी और वह लक्ष्य प्राप्ति की राह भी प्रशस्त कर सकेगी।