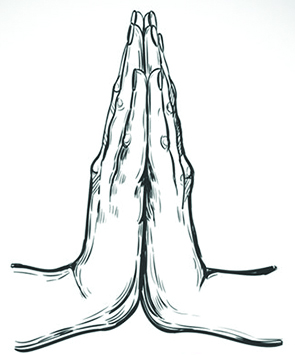
जैन संस्कृति में आस्त्रवों के प्रमुख पांच भेद माने गये हैं। जिनके कारण व्यक्ति के जीवन में ब्राह्म एवं आंतरिक प्रदूषण होते हैं:-
1. मिथ्यामिथ्यात्व(गलत धारणा)
2. अविरति(आत्मनुशासन का अभाव)
3. प्रमाद(जागरुकता का अभाव, लापरवाही, असावधानी)
4. कषाय(क्रोध, मान, कपट, लोभ आदि मानसिक संक्लेश)
5. अशुभ योग(मन, वचन, काय की निंदा एवं कुत्सित वृत्तियां)
क्षमा आगम संस्कृति(जैन संस्कृति) का सार है। क्षमा जीवन का आधार है। क्षमा आत्मिक मुक्ति का द्वार है। अंर्तमुखी याचना करता है और क्षमा प्रदान करता है, वो महान है। क्षमा भावना जैन संस्कृति की उपादेयता है। क्षमा क्षम धातु से बना है। इसके दो अर्थ हैं। 1. क्षमा का अर्थ है धैर्य, सहनशीलता 2. क्षमा सामथ्र्य वाचक है- सहने योग्य होना और पर्याप्त सक्षम होना। क्षमा मन की, विकारों की गांठें खोलती है। क्षमा से दया, सहानुभूति, संतोष, उदारता, मानव शून्यता, करुणा एवं मुदिता की भावनाओं को प्रोषित करती है। प्रश्न है कि पर्यावरण एवं सृष्टि संतुलन (इकोलॉजी)का सामंजस्य कैसे बढ़े? समस्या यही है कि कम सामग्री, आकांक्षा असीम है। यह सारा संघर्ष असीम-ससीम का है। उत्तराध्ययन सूत्र आगम के अनुसार इच्छा आकांक्षा के समान अनंत है। इच्छा के पात्र को कैसे भरें? पदार्थ से अपदार्थ, भोग से व्याधि की ओर चलें। क्षमाभाव अर्थात क्षमा याचना भी पर्यावरण शुद्धि का एक अनुपम मार्ग है, जिससे अंतर्मन की शुद्धि होती है। यही रास्ता है। संरक्षण में परिवर्तन हो सकता है। स्व-आलोचना के भाव से सकारात्मक दृष्टि रखते हुए विकारों प्रदूषणों से मुक्ति का मार्ग है, परस्पर क्षमा याचना दिवस पर्व। श्वेताम्बर परम्परा में क्षमा याचना पर्व आठ दिवसीय पर्यूषण पर्व की सम्पन्नता के साथ तथा दिगम्बर में क्षमा पर्व को दस लक्षण पर्व के रूप में मनाते हैं। जिसमें क्षमा, आर्जव, मार्दव, सत्य, संयम दस आध्यात्मिक तत्वों की विवेचना एवं साधना की जाती है। ताकि यह पर्व व्यक्ति को साधना शील बनाता है ताकि साधक की चेतना का रूपानान्तरण हो जाता है। व्यक्ति सरल, शुद्ध चित्त वाला बनकर पर्यावरण चेतना के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बन जाता है। जैन आगम उत्तराध्ययन 29/118 में कहा गया है-
खमावयाए णं जीवे पल्हायणभावं जणयई।
सव्वपाण-भय-जीव-सत्तेसु मित्तीभावमुप्पाएई।।
अर्थात क्षमा करने से भाव-चित्त में प्रसन्नता उत्पन्न होती है। इस क्षमावृत्ति से ही समस्त जीव योनि के प्रति मैत्री भाव प्रकट होता है। जिससे मन की मलीनता तिरोहित होती है। मन, स्वच्छ, निर्मल होता जाता है।
इसी प्रकार आगम दशवैकालिक सूत्र में कहा गया है-
उवसमेण हणे कोहं- अर्थात क्रोध को क्षमा से जीतना चाहिये।
स्थानांग 6 सूत्र आगम में प्रतिपादित किया गया है-उवसमसारं खु सामण्णं। अर्थात श्रमणत्व का सार है उपशमभाव, क्षमा।
आवश्यकसूत्र 4/22 में कहा गया है- खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में। मित्ती में सव्वभूएसु वेरं मज्झं न केणई।। अर्थात मैं समस्त जीवों को क्षमा करता हुंच सब जीव भी मुझे क्षमा करें। सबके प्रति मेरा मैत्रीभाव है। मेरा किसी के साथ भी वैर-विरोध नहीं है।
अत: सभी के साथ मैत्री करना चाहिये। मेत्ति भू एसु कप्पए
विवेचना:-
आगम उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन में 17वां सूत्र- क्षमापना के लिये हैं।
मूल प्रश्न- खमावणयाए णं भंते, जीवे किं जणयई?
समाधान-खमावणयाए णं पल्हायण भावं जणयई! पल्हायणभाव
मुवगए य सव्व-पाण-भूय-जीव-सत्तेसु मित्ती भाव मुप्पाएइ।
मित्ती भाव-मुव गए या वि जीवे भाव विसोहिं काऊण निब्भए भवइ।
अर्थात क्षमापना (क्षमा मांगने और क्षमा प्रदान करने) से चित्त में परम प्रसन्नता उत्पन्न होती है। प्रसन्न चित्त व्यक्ति संसार के सभी प्राणियों के साथ मैत्री भाव संपादन कर लेता है। मैत्री भाव से राग द्वेष का क्षय होकर, भाव विशुद्धि होती है। भाव विशुद्धि से व्यक्ति निर्भय हो जाता है। निर्भय होने से पर्यावरण संरक्षण होता है।
क्षमा भाव के सामने क्रोध की ज्वाला भी शांत हो जाती है। क्षमाभाव आत्म शांति, प्रफूलता का जीवंत मार्ग है। क्षमा मन की गांठे (विकार-प्रदूषणों) को खोलती है। इसे क्षमा वाणी पर्व भी कहा जाता है। क्षमा भाव, आत्म दर्पण का पर्व है, जिसमें व्यक्ति अपना स्वयं का आकलन करता है। अपनी वृत्तियों का स्व परीक्षण करता है। पर्यावरण चेतना एवं संरक्षण को जीवन में अपनाने का सुगम मार्ग है- क्षमा याचना।
क्षमायाचना पर्व का उद्देश्य है-आत्म शुद्धि क्योंकि पर्यूषण (आठ दिवस) पर्व अथवा दस लक्षण (दस दिवस) पर की गई साधना, संयम, तप व त्याग के परिणामस्वरूप पर्व के अंतिम दिवस पर आत्म चेतना को विकसित करने में व्यक्ति के रूपानांतरित होने में क्षमा याचना पर्व का विशेष महत्व है। यह पर्व आत्मोत्थान, जीवनोत्कर्षण के लिए अमोघ अस्त्र है। क्षमा याचना पर्व जीवन को मंगलमय तथा पर्यावरण विशुद्ध करता है। यह पर्व नर को नारायण बनाने की कीमियां (कला) सिखाने का अद्भुत पर्व है। इस आदर्शपरक पर्व की साधना का लक्ष्य होता है कि व्यक्ति में परिवर्तन टिकाऊ रहे। अर्थात् चिरंजीवी विकास का मूल मंत्र जैन संस्कृति में संयम सादगी एवं सदाचार है।
जैन संस्कृति के स्थानांग सूत्र के आगम में दस प्रकार के अहंकारों के प्रकार बतलाये गए है। (1) कुल-मद (2) गौत्र-मद (3) बल-मद (4) रूप-मद (5) तप-मद (6) श्रुत-मद (7) लब्धि-मद (8) ऐश्वर्य-मद (9) देवगमन-मद (10) अतिन्द्रिय ज्ञान-मद। किंतु क्षमायाचना पर्व व्यक्ति को झरने की भांति बनाता है क्योंकि वह गतिशील है, श्रमशील है, उपयोगी है, निर्मल है। जब मन की गांठे (विकार-प्रदूषण) क्षमा की अंर्तरंग गंगा में विलीन हो जाते हैं तब व्यक्ति सहज, सरल, पुलकित होकर सरस बनकर, शुद्ध चित्त वाला स्वत: हो जाता है।
मनुष्य का मस्तिष्क (न्यूरॉन्स) कचरे का डिब्बा नहीं है, जिसमें क्रोध, लोभ, मोह, मान और जलन जैसे कषायों का संग्रह करें। शुद्ध, विशुद्ध होकर अपने मस्तिष्क में क्षमा याचना के भाव से प्यार, सम्मान, ज्ञान, विज्ञान, मानवता, दया, करूणा, वात्सल्य जैसी बहुमूल्य निधि रखकर पर्यावरण चेतना एवं संरक्षण करें।
जैन संस्कृति के पांचवे आवश्यक सूत्र में कहा गया है कि मैं सब जीवों से क्षमा याचना चाहता हूं। सब जीव मुझे क्षमा करें। सभी जीवों से मेरी मित्रता हो। मेरा किसी से वैर न हो। जैन संस्कृति में मुनि/श्रावक/श्राविका को प्रतिदिन प्रात: एवं सायंकाल अवश्य करणीय है। क्षमा याचना पर्व के दिवस पर परस्पर, मन, वचन और काया से, जाने-अनजाने में किसी का दिल दुखाया हो अथवा संताप दिया हो तो ‘मिच्छामी दुक्कडम’ कहकर अपनी गलतियों की स्वीकारोक्ति की जाती है। जिससे व्यक्ति की सोच में परिवर्तन आता है। तब व्यक्ति सकारात्मक सोच, चिंतन, मनन से आप्लावित हो जाता है। यह सब क्षमा पर्व का परिणाम होता है। मैत्रीभाव की भावना रखने से, राग भाव गलता है। द्वेष भी विलुप्त होता है। मैत्री भाव की साधना जैन संस्कृति की साधना है जिससे संयम बढ़ता है। इसी भावना को सर्वमान्य तत्वार्थ सूत्र (7.6) में भी कहा गया है।
मैंत्री प्रमोद कारूण्य माध्यस्थानि सत्व गुणादिकल्लि श्यमाबिनाविनयेषु।
यानि कि प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव, गुणियों के प्रति प्रमोदभाव, दु:खियों के प्रति करूणाभाव तथा दोषियों के प्रति माध्यस्थ भाव रखना ही विशुद्धि का मार्ग है, संयम है। यही प्रदूषण निवारण का कारक है। यही अंत:करण क्षमा भाव से पर्यावरण चेतना एवं संरक्षण का केंद्र बिंदु है।
- डॉ.एनके खींचा, आरएएस(सेवानिवृत्त)